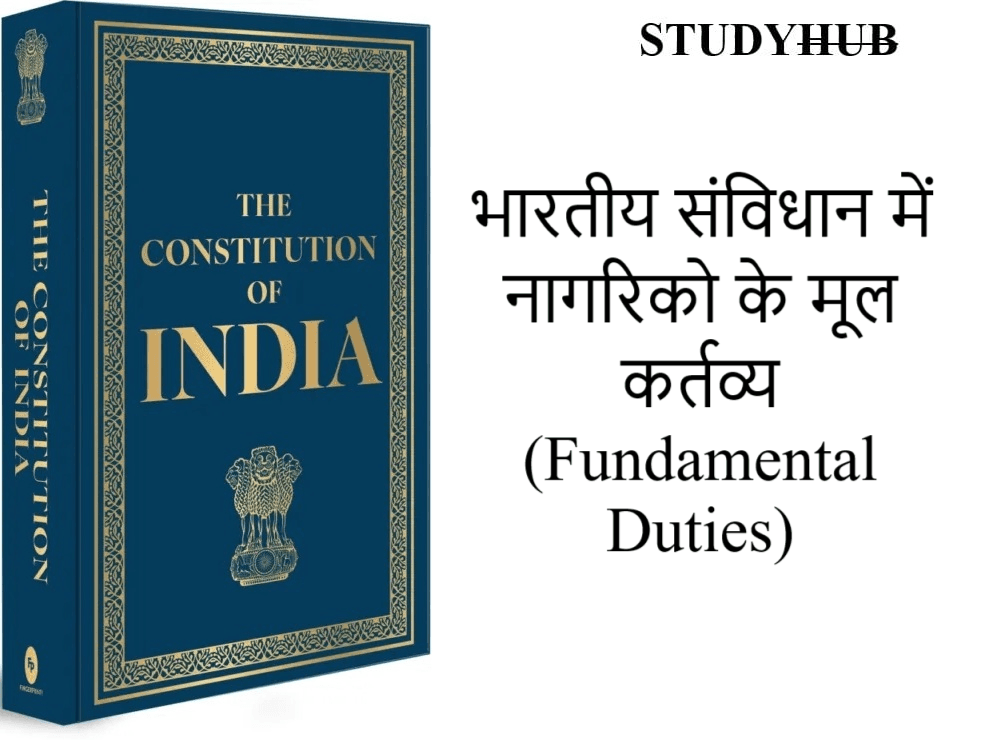
नागरिको के मूल कर्तव्य
सामान्य रूप से मूल कर्तव्य उन नागरिकीय नैतिक दायित्वों को इंगित करते हैं जो राष्ट्रभक्ति की भावना तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। समकालीन युग में कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तथापि, यह धारणा व्यापक रूप से मानी जाती है कि प्रत्येक अधिकार के अंतर्गत कर्तव्यों और दायित्वों का समावेश निहित होता है। अधिकार एवं कर्तव्य न केवल परस्पर तादात्म्यपूर्ण हैं, बल्कि ये दोनों पूर्णतः अविभाज्य भी माने जाते हैं। कर्तव्य, अधिकार का ऐसा मूलभूत पहलू है, जो किसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य है तो वहीं किसी अन्य के लिए वही अधिकार बन जाता है। उदाहरणार्थ, यदि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, तो यह सभी व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है कि वे मानव जीवन का सम्मान करें और किसी को हानि न पहुँचाएँ। यह मान्यता प्रचलित है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करे, तो अधिकार अपने आप संरक्षित रहेंगे; दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कर्तव्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति से ही अधिकारों को बल प्राप्त होता है।
संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provision)
भारत के मौलिक संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश नहीं था, किंतु वर्ष 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग-4 के उपरांत एक नया भाग-4क जोड़ा गया। इस संशोधन के अंतर्गत एक नवीन शीर्षक “मौलिक कर्तव्य” जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 51क में दस मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया।
बाद में, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में, मूल कर्तव्यों की कुल संख्या ग्यारह है।
मूल कर्तव्यों के स्रोत (Source of Fundamental Duties)
भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ की संविधानिक व्यवस्था से प्राप्त हुई थी। तथापि, भारतीय दार्शनिक परंपरा और सांस्कृतिक चिंतन में कर्तव्य-बोध को प्राचीन काल से ही प्राथमिक स्थान प्राप्त रहा है। वर्तमान समय में विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक राष्ट्रों में, जापान को छोड़कर किसी भी देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरणस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में नागरिकों के कर्तव्यों को सामान्य कानूनी मानदंडों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इसके विपरीत, साम्यवादी व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अग्रगण्य माना जाता है।
मूल कर्तव्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित वर्मा समिति (वर्ष 1999) ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 51क यह दर्शाता है कि ये धाराएँ उन मूल्यों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हैं, जो भारतीय परंपरा, पौराणिक आख्यानों, धार्मिक सिद्धांतों, तथा सांस्कृतिक आचरणों में सदा से विद्यमान रही हैं।
स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब हुआ था? (Swarn Singh Committee)
राष्ट्रीय आपातकाल (1975-77) की अवधि के दौरान, भारत सरकार द्वारा नागरिकों के कर्तव्यों की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए स्वर्ण सिंह समिति (वर्ष 1976) का गठन किया गया।
इस समिति ने अपनी सिफारिशों में यह महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किया कि नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि संविधान में मूल कर्तव्यों के लिए एक स्वतंत्र खंड को स्थान प्रदान किया जाए।
भारत सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार करते हुए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के अंतर्गत, संविधान में भाग-4क तथा एक नया अनुच्छेद 51क जोड़ा।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य (Fundamental Duties in Indian Constitution)
अनुच्छेद 51क के अंतर्गत, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह:
(क) संविधान के उद्देश्यों, संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान सहित समस्त संवैधानिक आदर्शों का सम्मानपूर्वक पालन करे।
(ख) स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणास्रोत रहे उच्च नैतिक आदर्शों को हृदयंगम करे और उनकी अनुपालना सुनिश्चित करे।
(ग) राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, एवं अखंडता की सुरक्षा करे और उसे अविचलित बनाए रखने का दायित्व निभाए।
(घ) भारत की रक्षा हेतु तत्पर रहे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा में सक्रिय भागीदारी करे।
(ङ) भारत के समस्त नागरिकों के मध्य सामाजिक समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना विकसित करे, तथा धर्म, भाषा, प्रांत, या वर्ग पर आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहते हुए ऐसी परंपराओं का परित्याग करे जो नारी सम्मान के विरुद्ध हैं।
(च) भारतीय समाज की संस्कृतिक गरिमा को समझे, उसका संवर्धन करे और संरक्षण हेतु प्रयासरत रहे।
(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झीलें, नदियाँ, और वन्यजीव सम्मिलित हैं, की रक्षा और संरचना करे, तथा समस्त जीवधारियों के प्रति करुणा भाव रखे।
(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, शिक्षा प्राप्ति, एवं सुधारवादी मानसिकता का विकास करे।
(झ) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसात्मक प्रवृत्तियों से दूरी बनाए रखे।
(ञ) अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में निरंतर उत्कर्ष की ओर प्रयत्नशील रहे जिससे राष्ट्र प्रगति, विकास, और उपलब्धियों की नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर सके।
(ट) यदि कोई व्यक्ति अभिभावक या संरक्षक है, तो छह से चौदह वर्ष की आयु वाले बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना उसका कर्तव्य होगा।
मूल कर्तव्यों की विशेषताएँ (Features of Fundamental Duties)
मूल कर्तव्यों का लागू होना केवल भारत के नागरिकों तक सीमित है।
इनमें से कुछ कर्तव्य नैतिक प्रकृति के हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित उच्च मूल्यों का पालन करना एक नैतिक दायित्व है, जबकि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं अहिंसा का पालन नागरिक उत्तरदायित्व की श्रेणी में आता है।
मूल कर्तव्यों की अवधारणा भारतीय संस्कृति, परंपरा, धर्म, एवं जीवन प्रणाली से गहराई से प्रभावित है।
ये न्यायालयों में सीधे प्रवर्तनीय नहीं हैं, अर्थात् इन्हें संवैधानिक अधिकारों की भाँति सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। इनका प्रभावी क्रियान्वयन केवल संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से किया जा सकता है।
मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन (Enforcement of Fundamental Duties)
- मूल कर्तव्यों को भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि कोई नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो उसे विधिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकता है।
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान कर सके।
- वर्मा समिति, जो नागरिकों के मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन पर गठित की गई थी, ने उन कानूनों, नियमों, और न्यायिक निर्णयों की पहचान की जो इन कर्तव्यों के परिपालन को सुनिश्चित करते हैं। कुछ प्रमुख विधिक प्रावधानों में निम्न शामिल हैं:
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: यह अधिनियम धर्म, जाति, या भाषा के आधार पर मतदान की माँग और भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955: यह अधिनियम जातिगत भेदभाव को अवैध ठहराता है।
- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971: इसके अंतर्गत संविधान, राष्ट्रगान, और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को निषिद्ध किया गया है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: यह अधिनियम वन्य प्रजातियों की संरक्षा का संविधानिक ढाँचा प्रस्तुत करता है।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980: इस अधिनियम का उद्देश्य वनों की अनियंत्रित कटाई और वन भूमि के दुरुपयोग पर नियंत्रण स्थापित करना है।
मूल कर्तव्यों से अपेक्षाएँ (Expectations From Fundamental Duties)
मूल कर्तव्यों का विश्लेषण करने पर इनमें समाहित गहन अपेक्षाएँ स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती हैं:
प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यवहार एवं कार्यकलापों को संविधान की विधिक सीमाओं के भीतर रखे, जैसे कि अस्पृश्यता का पालन करना निषिद्ध है।
संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है।
संवैधानिक संस्थाओं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, और संसद के प्रति आदरभाव रखा जाए।
राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज से संबंधित सरकारी निर्देशों का पालन करना अपेक्षित है।
स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले नेताओं द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों—जैसे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, और रंगभेद का विरोध, तथा लोकतंत्र और पंथनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों की अनुपालना की जानी चाहिए।
भारतीय संस्कृति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता, और अखंडता को प्राथमिकता दे, जबकि धर्म, भाषा, जाति, लिंग, अथवा जन्म स्थान को द्वितीय स्थान पर रखे।
नागरिकों को उन कुप्रथाओं का परित्याग करना चाहिए जो स्त्रियों की गरिमा को आहत करती हैं।
यद्यपि भारत एक सांस्कृतिक विविधता से युक्त राष्ट्र है, तथापि इसमें एक आंतरिक सांस्कृतिक एकता निहित है; अतः सभी नागरिकों को इस सामाजिक एकता के संवर्द्धन में सक्रिय योगदान देना चाहिए।
नागरिकों से यह भी अपेक्षित है कि वे अंधविश्वास, जड़ता, और अविवेक को त्यागते हुए जिज्ञासु, तार्किक, और विवेकशील दृष्टिकोण अपनाएँ।
साथ ही, उनमें मानवता, करुणा, और नैतिक मूल्यों का भी विकास होना चाहिए।
किसी भी सरकारी नीति का विरोध करते समय, नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सार्वजनिक संपत्ति को हानि न पहुँचाएँ, क्योंकि यह संपत्ति समस्त नागरिकों की सामूहिक धरोहर है।
अंततः, भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में स्थान दिलाने हेतु, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर सर्वोत्तम प्रयास करे।
मूल कर्तव्यों का महत्त्व (Importance of Fundamental Duties)
मूल कर्तव्य भारतीय न्यायपालिका को किसी विधि की संवैधानिक वैधता का मूल्यांकन करते समय एक प्रासंगिक संदर्भ प्रदान करते हैं।
ये कर्तव्य ऐसे किसी भी राष्ट्रविरोधी एवं समाजविरोधी कृत्य के प्रति सावधानी का संकेत देते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का दहन करना अथवा सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुँचाना।
इसके अतिरिक्त, ये कर्तव्य नागरिकों के लिए एक प्रेरक बल के रूप में कार्य करते हैं, जो उनमें अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, और राष्ट्रहित में सहभागिता की भावना का संचार करते हैं।
मूल कर्तव्यों के माध्यम से नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रयोग के समय राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यबोध का भी स्मरण कराया जाता है।
मूल कर्तव्यों की आलोचना (Criticism of Fundamental Duties)
आलोचकों का यह मत है कि मूल कर्तव्यों की विधिक प्रवर्तनीयता का अभाव इन्हें केवल नैतिक दिशानिर्देश या आदर्श वाक्य बना देता है।
इनमें समाहित कुछ कर्तव्यों को अस्पष्ट, बहुव्याख्यात्मक, एवं सामान्य नागरिकों के लिए बोधगम्य न माना गया है; उदाहरणस्वरूप—”उच्च आदर्शों“, “समग्र संस्कृति“, और “वैज्ञानिक दृष्टिकोण” जैसे पुनरावृत्तिपूर्ण शब्दों की अव्याख्यायिता।
कुछ संविधान विशेषज्ञों का यह तर्क है कि मूल कर्तव्यों की सूची में मतदान, कर भुगतान, एवं परिवार नियोजन जैसे अत्यंत आवश्यक सामाजिक दायित्वों का अवकाश इसे अपूर्ण बनाता है, यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने कर भुगतान को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी।
आलोचकों का यह भी विचार है कि इन कर्तव्यों को भाग-4 में शामिल कर उन्हें भाग-3 में न रखने से इनकी संवैधानिक स्थिति को गौण कर दिया गया, जबकि इन्हें मौलिक अधिकारों के समकक्ष स्थान देना उचित होता।
चूँकि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, अतः इन्हें नैतिक आदेशों की श्रेणी में स्थापित किया गया है। फिर भी, स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यपालन में विफलता की स्थिति में आर्थिक दंड एवं विधिक सज़ा का प्रस्ताव दिया था।
कुछ संविधान आलोचकों ने यह प्रश्न भी उठाया कि संविधान में ऐसे कर्तव्यों को शामिल करना उचित नहीं था जिन्हें उन व्यक्तियों पर भी लागू किया गया जो संविधान के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं। इससे इनकी व्यापकता, परंतु प्रभावशीलता संदिग्ध हो जाती है ।
