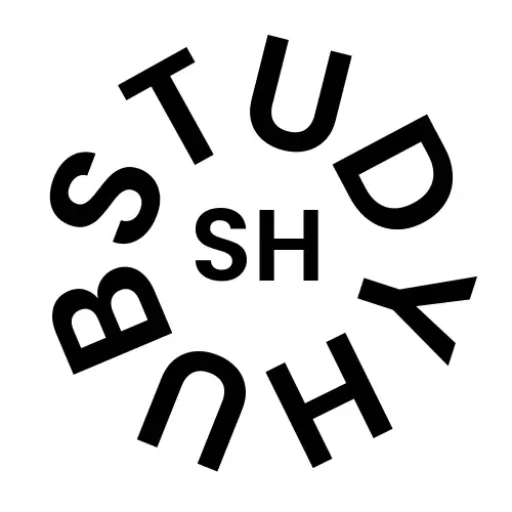मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण बौद्धिक, नैतिक, एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये अधिकार नागरिक को उसकी निजी पहचान गढ़ने और सर्वोत्तम हितों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो, मूल अधिकार मानव को गरिमामय और सम्मानजनक जीवन जीने की स्वतंत्रता के साथ-साथ उसकी प्राकृतिक प्रतिभा और दक्षताओं के विकास में भी सहायक होते हैं। यदि मूल अधिकारों की अनुपस्थिति हो, तो व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान अवरुद्ध हो जाता है, जिससे उसकी संपूर्ण क्षमताओं का समुचित विकास नहीं हो पाता।
अधिकारों के प्रकार (Types of Fundamental Rights)
- प्राकृतिक अधिकार – 17वीं और 18वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारकों का मत था कि मानवाधिकार प्रकृति या ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, जो कि राज्य की स्थापना से पूर्व से ही अस्तित्व में हैं। इन अधिकारों का जन्म मानव के साथ होता है, इसलिए किसी भी शासक या सत्ता द्वारा उन्हें छीना नहीं जा सकता। विचारकों ने तीन मौलिक प्राकृतिक अधिकार निर्धारित किए हैं – जीवन, स्वतंत्रता, और संपत्ति का अधिकार। अन्य सभी अधिकार इन्हीं मूलभूत अधिकारों से व्युत्पन्न होते हैं।
- मानवाधिकार – मानवाधिकारों की अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि केवल मनुष्य होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति कुछ निर्धारित अधिकारों का पात्र है। हर व्यक्ति एक विशिष्ट इकाई है और उसमें समान महत्व का निहितार्थ होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी अंतर्निहित मूल्यवत्ता के कारण स्वतंत्रता से जीने और अपनी संभावनाओं को पूर्णतया विकसित करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
- विधिक अधिकार – ये अधिकार प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। विधिक अधिकार उन अधिकारों को संदर्भित करते हैं जिन्हें राज्य द्वारा विधिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है –
I. संवैधानिक अधिकार, जो दो उप-श्रेणियों में विभाजित हैं – (क) मूल अधिकार, (ख) गैर-मूल अधिकार।
II. गैर-संवैधानिक अधिकार।
भारतीय संविधान में मूल अधिकार (Fundamental Rights in the Indian Constitution)
सामान्यतः, वे अधिकार जो संविधान में समाहित हैं और जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन्हें मूल अधिकार की संज्ञा दी जाती है। राज्य मूल अधिकारों की उत्पत्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि वह उनका संरक्षण करता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समावेश, स्वतंत्रता संग्राम की चेतना से जुड़ा हुआ है। उस समय के प्रमुख नेताओं ने यह संकेत दिया था कि स्वतंत्र भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, जैसे कि 1925 का कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, एवं 1931 का कराची अधिवेशन।
- मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग-3 में किया गया है।
- अनुच्छेद 12 से 35 तक, छह प्रकार के मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन मिलता है।
- भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं।
मूल अधिकारों की विशेषताएँ (Features of Fundamental Rights)
- मूल अधिकारों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है – कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए गए हैं।
- ये अधिकार राज्य की क्रियाओं के विरुद्ध प्रभावी होते हैं।
- मूल अधिकार अपने न्यायिक चरित्र के कारण अदालत द्वारा संरक्षित होते हैं।
- इन अधिकारों की सीमाएँ निर्धारित होती हैं; राज्य इन्हें युक्तिसंगत प्रतिबंधों के आधार पर सीमित कर सकता है।
- कुछ मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, जो राज्य की शक्तियों को संयमित करते हैं, जबकि कुछ सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, जो नागरिकों के हितों की रक्षा करते हैं।
- कुछ मूल अधिकारों का प्रवर्तन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी किया जा सकता है, जैसे कि अस्पृश्यता का उन्मूलन।
- ये अधिकार स्थायी या अविच्छेद्य नहीं हैं; संसद संविधान में संशोधन के माध्यम से इन अधिकारों को परिवर्तित या सीमित कर सकती है।
- अधिकतर मूल अधिकार स्वतः प्रवर्तनीय होते हैं, परंतु कुछ के लिए विधायी प्रक्रिया आवश्यक होती है, जैसे कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत।
राज्य की परिभाषा (Definition of State)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में ‘राज्य’ शब्द का प्रारूपिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ‘राज्य’ की परिधि में निम्नलिखित संस्थाएँ सम्मिलित की गई हैं—
भारत की संघीय सरकार एवं संसद,
प्रत्येक राज्य की सरकारी इकाइयाँ तथा विधानमंडल,
सभी स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ, जैसे कि नगरपालिकाएँ, पंचायतें, जिला परिषदें, सुधार न्यास, तथा वे निकाय जो विधियों, उपविधियों, आदेशों या अधिसूचनाओं का निर्माण अथवा प्रवर्तन करते हैं।
इसके अतिरिक्त, वे सभी संस्थान, चाहे वे संवैधानिक हों या गैर-संवैधानिक, जो सरकार के नियंत्रण में हों या उसके उपक्रम के रूप में कार्यरत हों, भी इस श्रेणी में आते हैं।
उच्चतम न्यायालय का यह मत निरंतर रहा है कि यदि कोई निजी संस्था या एजेंसी राज्य-सदृश दायित्व का निर्वहन कर रही हो, तो उसे भी अनुच्छेद 12 के अधीन ‘राज्य’ की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा।
मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ(Laws Inconsistent with or in derogation of Fundamental Rights)
अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का आधार स्तंभ माना जाता है। यह अनुच्छेद न्यायपालिका को इस अधिकार से सुसज्जित करता है कि वह किसी भी ऐसी विधि को निरस्त कर दे, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में हो। इस प्रकार, यह प्रावधान न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाता है। इस न्यायिक क्षमता को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है।
इस अनुच्छेद में यह सुस्पष्ट किया गया है कि संविधान के लागू होने से पूर्व भारत में प्रभावशील समस्त विधियाँ, यदि वे संविधान के इस भाग के किसी भी प्रावधान से विरोधाभासी हों, तो उस सीमा तक अमान्य होंगी।
इसी प्रकार, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को प्रतिबंधित या कमतर करे, और यदि बनाई जाती है, तो वह विधि केवल उसी सीमा तक अप्रभावी मानी जाएगी जितनी वह संविधान का उल्लंघन करती है।
अनुच्छेद 13 में ‘विधि’ शब्द की परिधि में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हैं—
- स्थायी विधियाँ, जैसे कि संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधियाँ।
- अस्थायी विधियाँ, जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश।
- कार्यपालिका द्वारा जारी विधियाँ जैसे- विनियम, नियम, अधिसूचनाएँ।
- विधिक मान्यता प्राप्त रूढ़ियाँ या परंपराएँ, जिनका विधि-सदृश प्रभाव हो।
उच्चतम न्यायालय द्वारा विधियों के अर्थ तथा परिधि को स्पष्ट करने वाले सिद्धांत(Principles Clarifying the meaning and scope of severability by the Supreme Court)
पृथक्करणयीता सिद्धांत (Doctrine of Severability)
जब किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक घोषित किया जाता है, तब यह प्रमुख प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या संपूर्ण अधिनियम को अमान्य कर दिया जाए अथवा केवल उस भाग को जो संविधान के प्रावधानों से विरोधाभासी है।
इस जटिल स्थिति से निपटने के लिए उच्चतम न्यायालय ने ‘पृथक्करणयीता सिद्धांत’ का प्रवर्तन किया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का वह अंश जो मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल है, उस अधिनियम के शेष भाग से प्रथक किया जा सकता है, और इस पृथक्करण से अधिनियम के मूल उद्देश्य पर कोई आघात नहीं होता, तो केवल असंगत अंश को ही असंवैधानिक घोषित किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को।
ध्यातव्य है कि “असंगति अथवा विरोध की सीमा तक” वाक्यांश से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी विधिक अधिनियम के केवल वे अंश अवैध माने जाएँगे जो मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल हैं या उनके साथ स्पष्ट विरोध में हैं; जबकि पूरे अधिनियम को निष्प्रभावी घोषित नहीं किया जाएगा।
आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse)
अनुच्छेद 13(1) में यह उपबंध किया गया है कि वे विधियाँ जो संविधान के प्रवर्तन से पूर्व प्रभाव में थीं, यदि वे मौलिक अधिकारों से असंगत हों, तो वे उस सीमा तक अवैध मानी जाएँगी।
उच्चतम न्यायालय ने यह व्याख्या दी है कि ऐसी विधियाँ संविधान के आरंभ से निरस्त नहीं मानी जातीं, बल्कि केवल उस समय से जब मौलिक अधिकारों की प्रभावशीलता प्रारंभ होती है, वे प्रवर्तनीय नहीं रह जातीं। यह विधियाँ पूर्णतः लोप नहीं होतीं, बल्कि वे केवल निष्क्रिय हो जाती हैं, चूँकि वे मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि जब तक ऐसे किसी अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया जाता या जब तक वह अधिकार निरस्त नहीं होता, तब तक वह विधि निष्क्रिय अवस्था में बनी रहती है, किंतु पूरी तरह से समाप्त नहीं होती।
अधित्यजन का सिद्धांत (Doctrine of Waiver)
अधित्यजन सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई भी नागरिक उन मूल अधिकारों को, जो संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता।
संविधान ने मूल अधिकारों को केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक जनहित के दृष्टिकोण से भी सम्मिलित किया है। ये अधिकार राज्य पर निर्धारित कर्त्तव्यों के रूप में आरोपित हैं, और किसी भी नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह राज्य को इन संवैधानिक दायित्वों से मुक्त कर दे।
भारतीय नागरिकों का एक विशाल वर्ग आज भी आर्थिक रूप से पिछड़ा है और शैक्षणिक एवं राजनीतिक चेतना की कमी के कारण अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। इस स्थिति में न्यायालय की यह प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि वह नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे और राज्य को उन दायित्वों से विमुक्त न होने दे, जो संविधान द्वारा उस पर अनिवार्य रूप से आरोपित किए गए हैं।