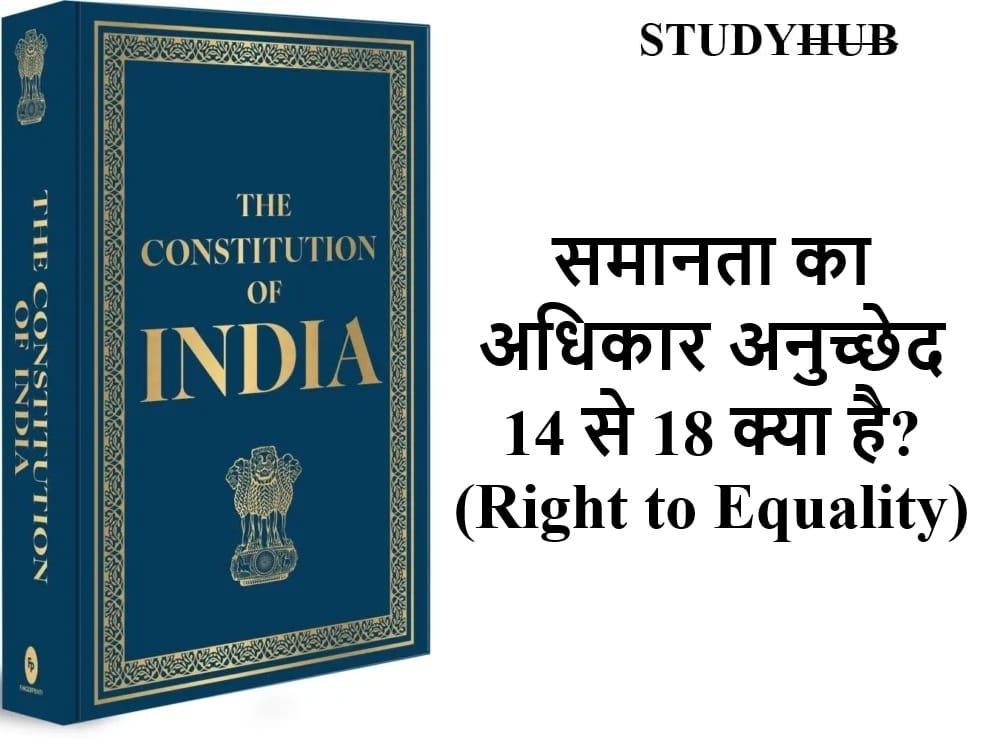
विधि के समक्ष समता (Equality before Law)
अनुच्छेद 14 के अनुसार, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को न तो कानून के समक्ष समानता से वंचित किया जा सकता है, और न ही विधियों के समान संरक्षण से। इस अनुच्छेद में दो पृथक वाक्यांश सम्मिलित हैं: प्रथम – ‘विधि के समक्ष समता’, एवं द्वितीय – ‘विधियों का समान संरक्षण’।
प्राकृतिक न्याय – इस अवधारणा से आशय उन न्यूनतम न्यायिक मानकों से है, जिनका पालन प्रत्येक प्रशासनिक व न्यायिक निकाय द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है, जब वे नागरिकों के अधिकारों अथवा विवादों से संबंधित निर्णय ले रहे हों।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मुख्यतः दो मौलिक तत्वों पर आधारित होते हैं –
I. कोई भी व्यक्ति अपने ही प्रकरण में न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभा सकता।
II. प्रत्येक पक्ष को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए; अर्थात्, बिना सुनवाई के दंड नहीं दिया जा सकता।
विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण में अंतर (Difference between Equality before Law and Equal Protection of Laws)
| विधि के समक्ष समता | विधियों का समान संरक्षण |
|---|---|
| ब्रिटिश विधिक प्रणाली से प्रेरित। | अमेरिकी संविधान से प्रेरित। |
| प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है; कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं। | समान परिस्थितियों में समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। |
| कानून सभी व्यक्तियों के प्रति एकसमान व्यवहार करेगा। | एकसमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत सभी के साथ एकसमान व्यवहार। |
| कोई भी व्यक्ति – अमीर या गरीब – कानून से ऊपर नहीं। | विनाभेद सम्मानपूर्वक समान व्यवहार। |
| यह एक नकारात्मक अवधारणा है। | यह एक सकारात्मक अवधारणा है। |
विधि का शासन (Rule of Law)
प्रोफेसर ए. वी. डायसी के अनुसार, विधि का शासन का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। समाज के प्रत्येक सदस्य – चाहे वह किसी उच्च पद पर हो या नहीं – सामान्य विधियों के अधीन होता है और न्यायालय की अधिकारिता में आता है। धन-धान्य से सम्पन्न व्यक्ति से लेकर आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक तक सभी पर समान विधि लागू होती है। डायसी के सिद्धांत के अंतर्गत तीन मौलिक अवधारणाएँ सम्मिलित हैं –
- मनमानी शक्ति का अभाव – किसी व्यक्ति को केवल विधिक उल्लंघन के आधार पर ही दंडित किया जा सकता है, न कि किसी व्यक्तिगत इच्छा या असंवैधानिक कृत्य के लिए।
- कानून के समक्ष समता – समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, या पद-प्रतिष्ठा में भिन्न क्यों न हो, विधि के अधीन समान होता है।
- संविधान का सामान्य विधि से उत्पन्न होना – यह धारणा भारत में प्रभावी नहीं है, क्योंकि भारत में नागरिकों के अधिकारों का प्रारंभिक स्रोत संविधान है, न कि सामान्य विधि।
समता के सिद्धांत के अपवाद (Exceptions of Rule of Equality)
अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समता का सिद्धांत पूर्णतः निरंकुश नहीं है; इसके कुछ विशिष्ट अपवाद भी हैं:
- राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान न्यायालयीय आदेश पारित नहीं किए जा सकते। उनके विरुद्ध कोई अभियोग चलाने से पूर्व दो माह की पूर्वसूचना देना अनिवार्य है।
- संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा सभा में कही गई बात या डाले गए मत के लिए किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं हो सकती। यह प्रावधान अनुच्छेद 105 तथा 194 के अंतर्गत संरक्षित है।
- विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, राजनयिक, एवं संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियाँ भारतीय न्यायालयों की नागरिक और दंडाधिकारी क्षेत्राधिकार से मुक्त होती हैं।
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध (Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion, Race, Caste, Sex or Place of Birth)
अनुच्छेद 15(1) के अनुसार, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा।
इस अनुच्छेद में प्रयुक्त ‘केवल’ और ‘विभेद’ शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
‘केवल’ का तात्पर्य यह है कि वर्जना केवल निर्दिष्ट आधारों पर लागू होती है, न कि किसी अन्य कारण पर।
‘विभेद’ से तात्पर्य है – किसी व्यक्ति के साथ अन्य की तुलना में विपरीत व्यवहार करना। यदि कोई कानून इन उल्लिखित आधारों पर असमान व्यवहार करता है, तो वह अवैध माना जाएगा।
अपवाद (Exceptions):
- राज्य, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, जैसे –
- स्थानीय संस्थाओं में महिला आरक्षण,
- मातृत्व अवकाश,
- बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
- राज्य, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे –
- शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क माफी,
- प्रवेश में छूट,
- आरक्षण संबंधी व्यवस्था।
ये संस्थान चाहे राज्य-सहायता प्राप्त, निजी, अथवा अल्पसंख्यक हों, सभी पर लागू हो सकते हैं।
अनुच्छेद 15(2)
कोई भी नागरिक, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इन में से किसी भी आधार पर –
(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन स्थलों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा;
(ख) राज्य द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्तपोषित अथवा सामान्य जनता के उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों, एवं सार्वजनिक स्थलों के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा।
इस उपखंड का प्राथमिक उद्देश्य भारत में व्याप्त अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन करना है।
अनुच्छेद 15(3)
इस उपबंध के तहत, राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करने की स्वतंत्रता दी गई है। उदाहरणस्वरूप –
- महिलाओं हेतु विशेष शैक्षणिक संस्थान,
- विशिष्ट कल्याणकारी योजनाएं।
अनुच्छेद 15(4)
यह खंड प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके अनुसार, अनुच्छेद 15 या 29(2) में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने से रोके। उदाहरण –
- नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण,
- छात्रवृत्तियाँ,
- प्रवेश में प्राथमिकता।
अनुच्छेद 15(5)
93वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा जोड़ा गया यह उपखंड राज्य को यह अधिकार देता है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों, तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान बना सके। यह नियम सभी राज्य-सहायता प्राप्त, निजी, एवं अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू हो सकता है।
लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान
अनुच्छेद 16(1)
यह उपबंध निर्धारित करता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में प्रत्येक भारतीय नागरिक को समान अवसर प्राप्त होगा।
अनुच्छेद 16(2)
राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के लिए धर्म, वंश, जातीय पहचान, लैंगिक भेद, स्रोत, जन्मस्थान, निवास स्थान अथवा इन तत्वों में से किसी एक के आधार पर किसी नागरिक को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता और न ही उससे भेदभाव किया जा सकता है।
टिप्पणी: राज्य के अधीन नियुक्ति अथवा नियोजन में अवसर की समानता के इस सामान्य सिद्धांत के चार अपवाद निर्धारित हैं।
अनुच्छेद 16(3)
संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि निर्माण कर किसी राज्य विशेष में निवास को सरकारी नियुक्तियों हेतु एक आवश्यक अर्हता घोषित कर सके, यद्यपि इसके लिए यथोचित औचित्य का होना अनिवार्य है।
अनुच्छेद 16(4)
राज्य यह अधिकार रखता है कि वह राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान करे, यदि यह पाया जाए कि ऐसे वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में पर्याप्त नहीं है।
अनुच्छेद 16(5)
किसी धार्मिक संस्था में कार्य करने वाले किसी कार्यान्वयन निकाय की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जा सकती है।
अनुच्छेद 16(6)
राज्य को यह विधिक छूट प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी नियुक्तियों अथवा पदों में, वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त, 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर सके।
टिप्पणी: अनुच्छेद 16 के प्रावधान संविदात्मक सेवाओं अथवा निजी क्षेत्र पर लागू नहीं होते।
आरक्षण से संबंधित प्रमुख शब्दों का अर्थ
पिछड़ा वर्ग : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े समुदायों की स्थिति की जाँच के लिये एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में काकालेलकर की अध्यक्षता में की गई थी, यद्यपि इसके द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 1979 में हुआ, जिसके अध्यक्ष बी.पी. मंडल थे। यह आयोग मंडल आयोग के नाम से व्यापक रूप से विख्यात है। आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।
इस आयोग ने 3743 जातियों को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया था। आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी, यह तर्क देते हुए कि इन वर्गों का शैक्षणिक एवं सामाजिक प्रतिनिधित्व अत्यंत अल्प है।
वर्ष 1990 में बी.पी. सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया, जिससे पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया।
वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने इस आरक्षण को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की।
क्रीमीलेयर (धनाढ्य पिछड़े वर्ग): इंदिरा साहनी वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमीलेयर की धारणा को प्रस्तुत किया। इसके अनुसार, पिछड़े वर्गों के संपन्न व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस श्रेणी में सरकार के ग्रुप-A एवं ग्रुप-B श्रेणी के अधिकारी सम्मिलित हैं।
सरकार समयानुसार क्रीमीलेयर के मानदंडों में परिवर्तन करती है। वर्तमान में इसकी वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख निर्धारित है। यह अवधारणा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर लागू नहीं होती।
बैकलॉग : जब किसी आरक्षित वर्ग के लिये निर्धारित पद किसी कारणवश रिक्त रह जाते हैं, तो वे बैकलॉग श्रेणी के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। बैकलॉग भर्ती, आगामी चयन प्रक्रिया में आरक्षित पदों के साथ सन्निहित हो जाती है।
पदोन्नति में आरक्षण : इंदिरा साहनी वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पदोन्नति में आरक्षण प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।
हालाँकि, 77वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1995) द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16(4क) को जोड़ा गया, जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार दिया गया।
इसके अतिरिक्त, 85वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2001) द्वारा इन वर्गों के लिए परिणामिक वरिष्ठता का नियम लागू किया गया।
एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद (2007) में उच्चतम न्यायालय ने तीन आधारों पर इस आरक्षण को वैध ठहराया—
- अनुसूचित जाति/जनजाति का पिछड़ापन,
- सेवाओं में उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व,
- तथा इससे प्रशासनिक दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव न पड़ना।
टिप्पणी: जर्नल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण वाद में मात्रात्मक आंकड़ों की आवश्यकता को हटा दिया गया।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Sections)
103वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को शासकीय नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की।
इस आरक्षण का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंतर्गत समाहित नहीं होते हैं।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये निर्धारित मूल्यांकन मापदंड निम्नलिखित हैं:
- परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कृषि भूमि की मात्रा 5 एकड़ से कम हो।
- आवासीय मकान का क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट से कम हो।
- नगरपालिका क्षेत्र में स्थित भूखंड की माप 100 वर्ग गज से अधिक न हो।
- नगरपालिका क्षेत्र से बाहर स्थित भूखंड 200 वर्ग गज से कम हो।
अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का उन्मूलन (Abolition of Untouchability)
अनुच्छेद 17 भारत में अस्पृश्यता के समूल अंत की घोषणा करता है और किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता संबंधी गतिविधियों को वर्जित घोषित करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले किसी भी कृत्य को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
यह प्रावधान भारत में सदियों से व्याप्त छुआछूत की सामाजिक प्रथा को समाप्त करने की महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था है। इस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों को समान सामाजिक सम्मान और सम्मानजनक जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।
अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 के अधिकार क्षेत्र में, संसद ने वर्ष 1955 में ‘अस्पृश्यता अपराध अधिनियम’ पारित किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य अस्पृश्यता से जुड़ी किसी भी सामाजिक गतिविधि को दंडनीय बनाना था। बाद में, वर्ष 1976 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसका नाम बदलकर ‘नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955’ कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा दंडात्मक प्रावधानों को अधिक कठोर और प्रभावी बना दिया गया।
यद्यपि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, किन्तु मैसूर उच्च न्यायालय ने एक वाद में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 17 में उल्लिखित अस्पृश्यता का अर्थ केवल शाब्दिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक सन्दर्भों में लिया जाना चाहिए। यह सामाजिक बुराई उस व्यवस्था की ओर संकेत करती है जिसमें कुछ जातियों को जन्म के आधार पर सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाता था या उन्हें न्यूनतर नागरिक के रूप में माना जाता था।
अनुच्छेद 18 : उपाधियों का उन्मूलन (Abolition of Titles)
अनुच्छेद 18 भारत में ब्रिटिशकालीन सामंती उपाधियों के प्रचलन को समाप्त करता है। उस काल में ‘महाराजा’, ‘राय बहादुर’, ‘राज साहब’, तथा ‘दीवान बहादुर’ जैसी उपाधियाँ दी जाती थीं, जो सामाजिक असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती थीं। यह अनुच्छेद इस प्रकार की सामंती परंपराओं को संविधान विरोधी मानते हुए निषिद्ध करता है क्योंकि ये समता के मूल अधिकार के प्रतिकूल हैं।
अनुच्छेद 18 चार प्रमुख उपबंधों के माध्यम से उपाधियों के निषेध को लागू करता है:
- राज्य, केवल सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियाँ प्रदान कर सकता है, अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी।
- भारत का कोई नागरिक, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।
- विदेशी व्यक्ति, जो भारतीय राज्य के अधीन कोई सार्वजनिक पद धारण करता हो, वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी विदेशी उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता।
- किसी भी व्यक्ति – चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी, यदि वह राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त है, तो वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी विदेशी उपाधि, पुरस्कार, उपहार या भेंट को स्वीकार नहीं कर सकता।
नोट : भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को उपाधियाँ नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन राष्ट्रीय सम्मानों की संवैधानिक वैधता को मान्यता दी है, क्योंकि ये कोई विशेषाधिकार या सामाजिक स्थिति नहीं प्रदान करते, बल्कि ये राष्ट्र के प्रति विशेष योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं।
